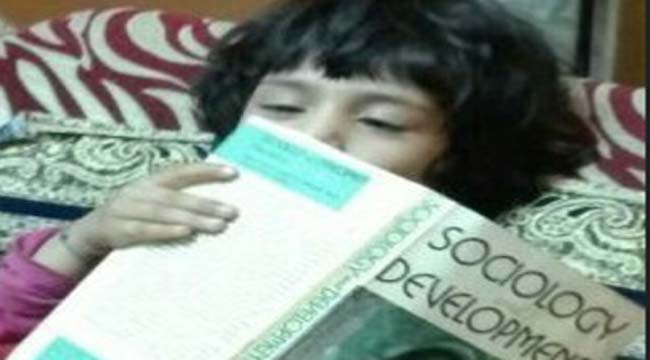हाल ही में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई आपदा ने एक बार फिर हिमालयी पारिस्थितिकी की नाज़ुकता और हमारी लापरवाहियों को उजागर कर दिया है। जान-माल की भारी क्षति हुई है, पर यह कोई नई कहानी नहीं। हम एक ऐसे चक्र में फंसे हैं — आपदा, मीडिया की सुर्खियाँ, राहत कार्य — और फिर भूल जाना।
शुरुआती रिपोर्टों में इसे क्लाउडबर्स्ट के कारण आई “प्राकृतिक आपदा” बताया गया। जल्द ही मीडिया का ध्यान राहत व बचाव कार्यों पर केंद्रित हो गया। लेकिन सवाल उठता है: क्या ये आपदाएं केवल प्राकृतिक हैं, या हम इन्हें और गंभीर बना रहे हैं?
वैज्ञानिक और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ अब इसके कारणों की पड़ताल करेंगे। वे शायद जल्दी चेतावनी प्रणाली और आपदा संभावित क्षेत्रों की मैपिंग जैसी सिफारिशें देंगे, जो ज़रूरी भी हैं। जैसा कि भूवैज्ञानिक और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख डॉ. पीयूष रौतेला कहते हैं, “हम बारिश नहीं रोक सकते, न ही हिमालय को समतल बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसे संस्थागत पुल बना सकते हैं जो वैज्ञानिक चेतावनियों को ठोस कार्यों में बदल सकें और जीवन बचा सकें।”
निर्माण कार्यों को लेकर भूवैज्ञानिक डॉ. दिनेश सती का कहना है कि मानसून में हिमालयी नदियों का जलस्तर सामान्य से दस गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में किसी भी निर्माण को उच्च बाढ़ स्तर (HFL) से ऊपर होना चाहिए। लेकिन सड़कें, पुल, और जलविद्युत परियोजनाएं बिना सोचे-समझे नदियों और ढलानों पर बनती जा रही हैं।
2012 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगोत्री से उत्तरकाशी तक 41 किमी क्षेत्र को भागीरथी ईको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया। इसमें धराली समेत 88 गांव शामिल थे (धराली क्रम संख्या 18 पर)। इस क्षेत्र में नए बांध, खनन, पेड़ कटाई, औद्योगिक इकाइयों और सड़क निर्माण पर रोक लगाई गई थी। पर स्थानीय जनता ने इसे विकास पर रोक मानते हुए इसका विरोध किया।
तत्कालीन राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्णय का विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे सीमावर्ती गांवों से पलायन बढ़ेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। यह क्षेत्र चार धाम यात्रा मार्ग में आता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे पहले से ही भारी दबाव है।
बात सिर्फ एक अधिसूचना या विरोध की नहीं है। यह एक गहरी टकराव की कहानी है — विकास की मांग और पर्यावरण संरक्षण की ज़रूरत के बीच।
2006 से ही समाजसेवी संगठनों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने ऊपरी हिमालय क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं और भारी निर्माण कार्यों के ख़तरों को उजागर किया है। मानवीय गतिविधियों का बोझ बढ़ता जा रहा है — और इसके साथ बढ़ रही है तबाही।
आज जब धराली खबरों में है, तब यह याद रखना ज़रूरी है कि इसकी चेतावनी वर्षों पहले दी जा चुकी थी — वैज्ञानिकों और जागरूक नागरिकों द्वारा। लेकिन इन आवाज़ों को अक्सर अनसुना कर दिया गया।
उत्तराखंड की आपदाएं अब एक पहचानी हुई पटकथा बन गई हैं: क्लाउडबर्स्ट, बाढ़, भूस्खलन, भूमि धंसना, फिर राहत कार्य और मुआवजे की घोषणाएं। पर असली मुद्दा — टिकाऊ विकास बनाम तात्कालिक विकास — जस का तस है।
एक समाजशास्त्री के रूप में, मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे पूर्वज सदियों तक हिमालय में कैसे रहते थे। उन्होंने भी भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक विपदाएं देखी होंगी, पर उनके जीवन में प्रकृति के साथ सामंजस्य था। आज हमने उस संतुलन को तोड़ दिया है।
भागीरथी फिर पुकार रही है। सवाल यह है — क्या कोई सुन रहा है?
देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी एक समाजशास्त्री हैं, जो 40 वर्षों से NGO और विकास क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र हैं और उनके शोध कार्य का उल्लेख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तकों में भी हुआ है।